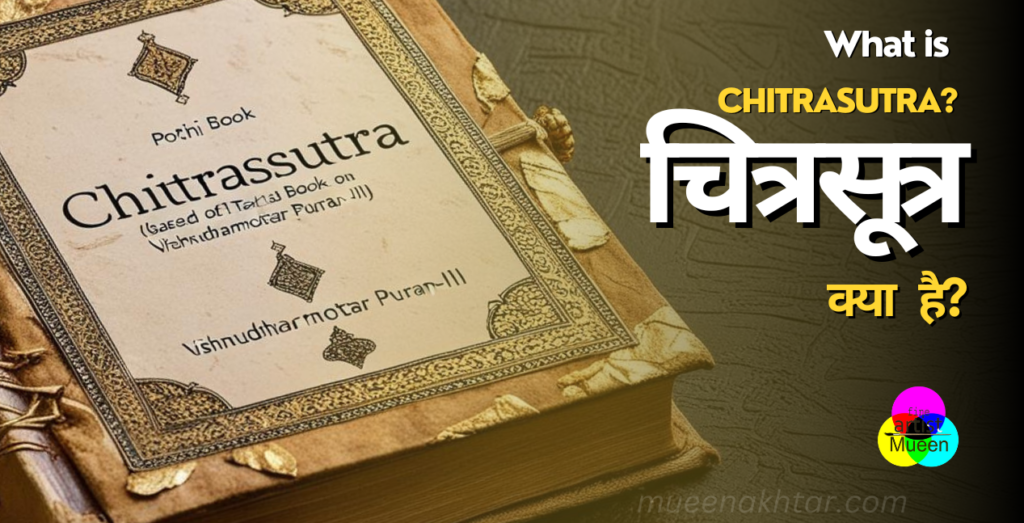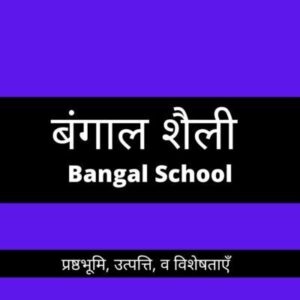भारतीय चित्रकला में कला सिर्फ़ कला नहीं है, बल्कि कला हमारे अध्यात्म से जुड़ी है। अतः चित्रसूत्र (Chitrasutra) भारतीय चित्रकला का एक महान व विशेष ग्रंथ है। चित्रसूत्र (Chitrasutra) का नाम हर भारतीय चित्रकारों ने, कला विद्वानों ने व कला छात्रों ने अपने जीवन में कई बार सुना होगा। तो चलिए इस लेख में चित्रसूत्र (Chitrasutra) के विषय में विस्तार से समझते हैं कि चित्रसूत्र क्या है?
चित्रसूत्र (Chitrasutra) क्या है?
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के भाग तीन के 35 से 43 तक के अध्याय, चित्रसूत्र कहलाते हैं। शरीर रचना से लेकर रंगों के बनाने तक के निर्देश चित्रसूत्र (Chitrasutra)में चित्रकला के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी है। इन अध्यायों में या कहें तो चित्रसूत्र में दिए गए हैं।
अब सवाल उठता है की यही अध्याय (35 से 43) ही चित्रसूत्र क्यूँ कहे जाते हैं। दूसरा सवाल के चित्रसूत्र नाम किसने दिया। तो इन सवालों का जवाब भी विष्णु धर्मोत्तरपुराण भाग-III के अध्याय 35 में मिलता है। यहाँ मार्कण्डेय मुनि राजा वज्र से कहते हैं की अब मैं आपको चित्रसूत्र (Chitrasutra) बताता हूँ। इसके बाद वे श्लोकों के द्वारा चित्रकला से सम्बंधित सारी जानकारी देते हैं। आगे के अध्याय ४३ में मार्कण्डेय मुनि चित्रकला के नियमों व सुझावों की विवेचना को समाप्त करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ चित्रसूत्र समाप्त होते हैं। अतः विष्णु धर्मोत्तरपुराण भाग-III के अध्याय ३५ से ४३ चित्रसूत्र कहे जाते हैं। चित्रसूत्र को चित्रसूत्र नाम देने वाले मार्कण्डेय मुनि ही हैं।
मेरा मानना है कि शरीर रचना का जितनी सटीक व उपयुक्त वर्गीकरण, स्वभाव, मुद्राएँ आ उनकी माप चित्रसूत्र (Chitrasutra) में बतायीं गयीं है, वो आज तक चित्रसूत्र के अलावा कहीं ओर नहीं मिलतीं। हर भारतीय चित्रकार को कम से कम जीवन में एक बार चित्रसूत्र (Chitrasutra) का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए।
(Chitrasutra) श्रोत या उत्पत्ति
- चित्रसूत्र (Chitrasutra) की उत्पत्ति विष्णुधर्मोत्तर पुराण से ही मानी जाती है।
- यह राजा वज्र व मुनि मार्कण्डेय के बीच की वार्तालाप के रूप में हमें देखने को मिलता है।
- वास्तव में चित्रसूत्र (Chitrasutra), पूर्व में पुराणों व ग्रंथों में उल्लेखित चित्रकला के नियमों का संकलन है।
- दुर्भाग्य से पूर्व का साहित्य अब मिलना दुर्लभ है। इसलिए ललित कलाओं से सम्बंधित यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
- विष्णुधर्मोत्तर प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण, चित्रकला और प्रतिमा निर्माण के सिद्धांत और अभ्यास पर उपलब्ध सबसे पुराना संपूर्ण ग्रंथ है।
- चित्रसूत्र को ओर अधिक समझने के लिए हमें विष्णुधर्मोत्तर पुराण पर चर्चा करनी होगी।
विष्णुधर्मोत्तर पुराण

विष्णुधर्मोत्तर पुराण की बात करें तो ये विष्णु पुराण का एक उपपुराण है। माना जाता है कि इसे विष्णु पुराण में बाद में जोड़ा गया था। यह पुराण लगभग 6वीं शताब्दी या कुछ बाद का ग्रंथ है। इसके तीन खंड (भाग) हैं जिसमें लगभग 16 हज़ार श्लोक हैं। खंड या इनके भाग के अनुसार इनमे उल्लेखित विषय व अध्याय इस प्रकार हैं:
प्रथम खंड- (269 अध्याय) इस भाग में संसार की उत्पत्ति, भूगोल, ज्योतिष, वंशावलियाँ (राजाओं व ऋषियों की) अप्सराओं का उल्लेख, शंकर गीत, श्राद्ध व व्रत के बारे में बताया गया है।
द्वितीय खंड– (183 अध्याय) इस भाग में ज्योतिष, धर्म, राजनीति, औषधि विज्ञान, व मानव जीवन से सम्बंधित बातें के बारे में बताया गया है।
तीसरे खंड– (118 अध्याय) इस भाग विशेष रूप से कला व साहित्य से समन्धित है। इसमें ललित कलाओं जैसे चित्रकला, नृत्य, संगीत, वास्तु शिल्प, साहित्य, काव्यशास्त्र, छंदशास्त्र व संस्कृत व प्रकृत भाषा का व्याकरण आदि के बारे में विस्तार से वर्णन है।
चित्रसूत्र की विषयवास्तु
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के भाग(खंड) तीन के 35 से 43 तक के अध्याय को चित्रसूत्र कहा जाता है। अध्याय के अनुसार चित्रसूत्र की विषय वास्तु इस प्रकार है:
अध्याय 35, (श्लोक 1-18)
- मुनि मार्कण्डेय ने चित्र के नियमों के बारे में बताया।
- मुनि मार्कण्डेय के अनुसार ऋषि नारायण ने संसार के कल्याण के लिए चित्र के नियम विकसित किए थे।
- नृत्य और चित्र दोनों ही समान रूप से श्रेष्ठ माने गए हैं।
- इसमें पाँच प्रकार के पुरुष बताए गए हैं साथ ही उनकी ऊँचाई के साथ शरीर के प्रमुख हिस्सों की नाप भी बतायी गयी है:
- हंस (Hamsa) (माप -100 अंगुल)
- भद्र (Bhadra) (माप -106 अंगुल)
- मालव्य (Malavya) (माप -104 अंगुल)
- रुचक (Euchaka) (माप -100 अंगुल)
- शशक (Sasaka) (माप -90 अंगुल)
अध्याय -36 (शरीर के प्रत्येक अंग का माप)
- इसमें शरीर के सभी छोटे बड़े अंगों की नाप विस्तारपूर्वक बतायी गयी है।
- नाप के साथ-साथ पाँच प्रकार के पाँच प्रकार पुरुषों (जो पहले बताए जा चुके हैं) के लक्षण भी बताए गए हैं। जो आगे उल्लेखित हैं:
- हंस पुरुष को बलवान बनाना चाहिए, जिसकी भुजाएँ साँपों के राजा जैसी हों।
- हंस का रंग गोरा हो व आँखें आकर्षक हों। उसका चेहरा सुंदर हो, कमर सुंदर हो और उसकी चाल हंस जैसी हो।
- भद्र को उच्च आत्मा वाला बताया गया है। इस प्रकार के पुरुषों के कदम हाथी के समान होते हैं। इनका माथा बालों वाला होता हैं। इनकी पूर्ण विकसित और झुकी हुई गोल भुजाएँ होनी चाहिए।
- मालव्य का रंग मूंग के समान काला होता है। इसकी पतली कमर के कारण उसका शरीर बहुत सुंदर होता है। इस प्रकार के पुरुषों की भुजाएँ घुटनों तक पहुँचती हैं। चौड़े कंधे, चौड़े जबड़े और हाथी जैसी नाक होती है।
- ‘रुचक’ के बारे में कहा जाता है कि वह सत्यवादी, उच्च आत्मा वाला, बलवान और चतुर होता है, जिसकी गर्दन शंख के समान होती है और रंग शरद ऋतु के समान श्वेत (सफ़ेद) होता है।
- ‘शशक’ के बारे में कहा जाता है कि वह चतुर होता है। इसका जिसका रंग थोड़ा भिन्न होता है जिसके गाल भरे हुए और आंखें मीठी होती हैं। इस पुरुष का रंग लाल-काला बताया गया है।
(Chapter) अध्याय -37 (श्लोक 1-17)
- इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है। मार्कण्डेय ने बताया कि पुरुष पाँच प्रकार के होते हैं, वैसे ही स्त्रियाँ भी पाँच प्रकार की होती हैं। आगे इस अध्याय में स्त्रियों के चित्रण के विषय में निर्देश दिए गए हैं।
- इस अध्याय में राजाओं को चित्रित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। राजाओं को चित्रण सम्बन्धी निर्देशों का वर्णन करते हुए राजाओं के बालों के प्रकार भी बताए गए है। इस अध्याय में राजाओं के निम्नलिखित 6 प्रकार के बाल बताए गए हैं:
- कुंतल, (ढीले) बाल,
- दक्षिणवर्त, दाईं ओर मुड़े हुए,
- तरंगा (लहरदार),
- सिंहकेसर (अयाल जैसा),
- वरधारा (विभाजित), और
- जटातासर (जटा)।
(Chapter) अध्याय 39, (श्लोक 1-32)
- मार्कण्डेय ने इस अध्याय में शरीर की विभिन्न मुद्राएँ व भेद बताए हैं। ये स्थितियाँ या भेद कुल मिलाकर नौ हैं।
- साथ ही इनकी प्रकृति बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।
- रज्वागत (सीधी)
- अनृजु (जो सीधी ना हो)
- सचीक्कतशरीर (मुड़े हुए शरीर के साथ)
- अर्धविलोचन (आधी आँखों वाली)
- पार्श्वगत (पार्श्व से व्युत्पन्न)
- परावृत्त (गाल-मुड़ा हुआ” गोल स्थिति आती है)
- पृष्ठागत (फिर पीछे का दृश्य या पीठ से व्युत्पन्न)
- परिवृत्त (गोल मुड़ा हुआ स्थिति)
- समानत (पूरी तरह से झुका हुआ है)
अध्याय 39, (श्लोक 34-51)
- इस अध्याय में क्षय-वृद्धि (घटना-वृद्धि) की आनुपातिक माप के नियमों बारे में बताया गया है।
- ये दो प्रकार की हैं:- चित्र (सरल) और विचित्र (विविध)।
- यह वृद्धि तथा क्षय का का सम्बंध शरीर तथा उसके विभिन्न अंगों में है।
- इस अध्याय में ये तेरह प्रकार के बताए गए हैं।
- मार्कण्डेय ने क्षय-वृद्धि का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है ,
“एक विद्वान कलाकार को अपनी बुद्धि की मदद से, क्षय और वृद्धि के साथ आनुपातिक माप का उपयोग करना चाहिए”।
अध्याय (Chapter) – 40, (श्लोक 1-30)
- इसमें भित्तचित्रण हेतु पृष्ठ-भूमि व रंगों को तैयार करने की सम्पूर्ण विधि बतायी गयी है।
- दिवार की सतह को तैयार करने की विधि बतायी गयी
- यह अध्याय भित्त पर रेखांकन करने के तरीके को इस अध्याय में बताया गया है।
- रंगों के पदार्थ व उनको बनाने के विधि के साथ ही तूलिका के विषय में भी उल्लेख मिलता है।
अध्याय(Chapter) 41, (श्लोक 1-15)
- मार्कण्डेय ने समाज में मनुष्यों के प्रकार बताए हैं। उन्होंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं:
- (1) सत्य (उचित अनुपात के सुंदर शरीर वाले, लम्बे लोग)
- (2) वैणिक (वनीय)-(व्यापारी, सौदागर और कृषि उत्पादन में शामिल लोगों को वैश्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था)
- (3) नागर (शहर का या आम आदमी)
- (4) मिश्र (मिला हुआ-मिश्रा)
- इस अध्याय में रेखांकन व छाया प्रकाश के विषय में भी बताया गया है।
- रेखांकन में छाया प्रकाश अंकित करने की तीन विधियाँ बतायीं गयीं है:
- (1) पतरजा- रेखाओं को पार करना (शाब्दिक रूप से पत्तियों के आकार की रेखाएँ, पटराजा),
- (2) ऐरिका (स्टंपिंग)
- (3) विंदुजा (डॉट्स द्वारा)
- इसमें चित्रों के दोष के साथ साथ चित्रों को उन्हें और आकर्षक बनाने की बातें बतायीं गयीं है।
(Chapter) अध्याय 42, श्लोक 1-84.
रूप निर्माण
- राजाओं, ऋषि, गंधर्व, दैत्य, दानव, मंत्री, ब्राह्मण, संवत्सर और कुल पुरोहित आदि के आकार व रूपों की जानकारी दी गयी है।
- इन रूपों के साथ उनके लक्षण व वर्ण के अनुसार उनकी वेशभूषा का भी इसमें वर्णन किया गया है।
- मुनि मार्कण्डेय के अनुसार दैत्यों, दन्नवों, यक्षों और ऋक्षों की पत्नियाँ और माताएँ अपने पुरुषों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए। यही बात पिशाचों की पत्नियों के लिए भी लागू होती है।
- समाज की विभिन्न वर्गों की स्त्रियों को बनाए जाने के निर्देश बताए गए हैं।
- विभिन्न स्त्रियों में विधवा, कुबड़ी, बूढ़ी, बोनी, शाही, आधि स्त्रियों को चित्रित करने के सुझाव दिए बताए गए हैं।
- जैसे कि विधवाओं को आभूषणों के बिना, सफ़ेद बालों के साथ सफ़ेद कपड़े पहने दिखाया जाना चाहिए।
- वहीं कुबड़ी, बौनी और बूढ़ी महिला को भी उनकी प्राकृतिक अवस्था में दिखाया जाना चाहिए।
- स्त्रियों के अलावा अलग अलग व्यवसाय के पुरुषों को बनाने के भी सुझाव इस अध्याय में बताए हे हैं।
- जैसे कि पैदल सैनिकों को वर्दी में, व्यापारियों को उनके सिर को चारों ओर से पगड़ी से ढके हुए दिखाया जाना चाहिए।
- अच्छे संगीतकार, नर्तकों एक शानदार पोशाक पहननी चाहिए।
- देश और शहर के सबसे सम्मानित लोगों को भूरे बालों के साथ चित्रित किया जाना चाहिए।
- पहलवानों को चौड़े कंधों, मांसल अंगों, मोटी गर्दन के साथ दिखाया जाना चाहिए।
- ये छोटे बालों के साथ, अभिमानी और उतावले देखाई देना चाहिए।
प्राकृतिक चित्रण व जीव-जंतु चित्रण
- जानवरों के चित्रण के बारे में मार्कण्डेय कहते हैं कि बैल, शेर और अन्य जानवरों को उचित परिवेश में दिखाया जाना चाहिए।
- जैसा कि वे प्रकृति में दिखाई देते हैं वेसा ही उन्हें बनाया जाय।
- प्राकृतिक चित्रण के विषय में भी मुनि मार्कण्डेय ने कहा के देखाई देने वाली चीजें उनके स्वाभाविक रूप में बनायीं जाय।
- आकाश पक्षियों से भरा हो। प्राकृतिक कई चीजों के विषय में उन्होंने चित्रण सम्बन्धी कई सारे सुझाव दिए।
- इसके अलावा इस अध्याय में नदी (समुद्र), शहर, गावों, किलों, बाज़ार, जुआ घर, मधुशाला, युद्ध के मैदान आदि को चित्रण करने के सुझाव दिए गए हैं।
अध्याय 43, श्लोक 1-39
- इस अध्याय में मार्कण्डेय ने भावों व रसों के बारे में बताया।
- चित्रकला में दर्शाए गए भाव (रस) नौ हैं, अर्थात, श्रृंगार, हास्य, करुणा, वृहद, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और अनंत।
- चित्रकला के आठ (अच्छे) गुण बताए गए हैं।
- जैसे कि उचित स्थान, अनुपात और अंतराल, सुन्दरता और स्पष्टता, समानता, कमी और वृद्धि या छोटा होना।
- धर्मी और शास्त्रों में पारंगत लोगों द्वारा बनाया गया चित्र समृद्धि लाता है और विपत्ति को बहुत जल्दी दूर करता है।
- चित्र चिंता को दूर करता है, भविष्य में अच्छाई लाता है।
- चित्र अद्वितीय और शुद्ध आनंद देता है, बुरे सपनों की बुराइयों को मारता है।
- चित्र घर के देवता को प्रसन्न करता है।
- जहां चित्र को विशेष रूप से रखा जाता है, वह खाली नहीं लगता।
- चित्रकला के नियम लोहे, सोने, चाँदी, ताँबे और अन्य धातुओं की नक्काशी के लिए मान्य हैं।
- मूर्तिकला में भी चित्रकला के नियम लागू होंगे चाहे मूर्ति पत्थर की हो, धातु या लकड़ी की हो।
- अंत में मार्कण्डेय मुनि कहते हैं कि चित्रकला के ये केवल सुझाव हैं।
- इनका वर्णन अगर विस्तार से किया जाय तो कई वर्ष काम पढ़ जाएँगे।
- जो भी सुझाव या नियम यहाँ उल्लेखित नहीं है, उनको नृत्य कला से लिया जाना चाहिए।
- अंत में राजा वज्र से चित्रकला के महत्व को बताते हुए मार्कण्डेय मुनि कहते हैं:
कलानां प्रवरं चित्रं, धर्मकमार्थमोक्षदम् , मांगल्य प्रथमं चैतद्, ग्रहेयत्र प्रतिष्ठतम।।
यथा सुमेरु: प्रवरो नागानाम्, यथांडजानां गरुड़: प्रधान:। यथा नराणां प्रावर: क्षितीश:, तथा कलानामिह चित्रकल्प:।।
अर्थात् चित्रकला सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है। ये धर्म और मुक्ति के देने वाली है। इसे घर में रखना बहुत शुभ होता है। जैसे सुमेरु, पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है, गरुड़, पक्षियों में श्रेष्ठ है। राजा, मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वैसे ही चित्रकला सभी कलाओं में सर्वश्रेष्ठ है।